इमरजेंसी के पचास साल: मीडिया पर तानाशाही की पकड़ या प्रतिरोध की गूंज
(आलेख: हरिशंकर पाराशर)

इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लागू की गई इमरजेंसी को पचास साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दौर की एक प्रमुख छाप आज भी प्रेस की स्वतंत्रता पर हुए अभूतपूर्व हमले के रूप में बनी हुई है। उन इक्कीस महीनों में प्रेस का दमन और सेंसरशिप की कठोर व्यवस्था स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। अखबारों और पत्रिकाओं के पन्ने काले रंग से पुते हुए या खाली छोड़े गए, जो सेंसरशिप की कैंची का शिकार हुए। यह वह दौर था जब एक औपचारिक सेंसरशिप तंत्र बनाया गया, जिसका मकसद हर छपने वाले शब्द को सरकार की मर्जी के मुताबिक ढालना था। उस समय मास मीडिया का दायरा मुख्यत: पत्र-पत्रिकाओं तक सीमित था। रेडियो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था, टीवी अपने प्रारंभिक दौर में था, और सिनेमा जैसे स्वतंत्र माध्यम को भी काबू करने की कोशिशें हुईं।

यह सब उस समय के भारत के लिए नया और अपरिचित था।लेकिन यह मानना ठीक नहीं होगा कि इमरजेंसी में प्रेस पूरी तरह दब गया। सेंसरशिप का थोपा जाना इस बात का सबूत था कि प्रेस ने हार नहीं मानी थी। काले रंग से रंगे या खाली छोड़े गए पन्ने न केवल दमन की कहानी कहते थे, बल्कि प्रतिरोध की एक शानदार गाथा भी रचते थे। कई अखबारों और पत्रिकाओं ने शुरुआती दिनों में पूरे पन्ने खाली या काले करके सेंसरशिप के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। यह प्रेस का साहस था, जो तानाशाही के सामने झुकने से इनकार कर रहा था।बेशक, प्रेस की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। भारतीय प्रेस की विविधता उस दौर में भी साफ दिखती थी। कुछ प्रकाशनों ने प्रतिरोध का रास्ता चुना, तो कुछ समय के साथ इमरजेंसी को सामान्य मानने लगे। शुरुआती झटके के बाद इमरजेंसी का एक तरह से सामान्यीकरण होने लगा था। फिर भी, अधिकांश प्रेस का रुख इमरजेंसी के खिलाफ ही रहा।

इसे एक असामान्य स्थिति माना गया, जिससे छुटकारा पाने की प्रतीक्षा थी।1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी इमरजेंसी की करारी हार में प्रेस के इस विरोधी रुख की कितनी भूमिका थी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह स्पष्ट है कि इमरजेंसी की हार का एक बड़ा कारण जनता की आवाज का सत्ता तक न पहुंचना था। प्रेस, जो जनता और सत्ता के बीच सेतु का काम करता है, उस दौर में सेंसरशिप की वजह से खामोश कर दिया गया था। इंदिरा गांधी को जीत की उम्मीद थी, लेकिन जनता ने उन्हें इस कदर खारिज किया कि कांग्रेस उत्तरी भारत में मात्र दो लोकसभा सीटों पर सिमट गई।वरिष्ठ पत्रकार मानिनी चटर्जी ने एक बार बताया था कि 2004 के चुनाव में भी सत्ताधारी पार्टी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 1977 और 2004 की हार में एक बड़ा अंतर था। 1977 में सत्ता को जनता की नब्ज का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि प्रेस सेंसरशिप की जकड़न में था। वहीं, 2004 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में झुका हुआ था, जनता की राय को ठीक से भांप नहीं पाया।पिछले पचास सालों में, खासकर पिछले दो दशकों में, भारत का मीडिया परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। पिछले दस सालों में यह बदलाव और तेज हुआ है।

पहला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पारंपरिक प्रिंट मीडिया को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा, बड़े पूंजीपतियों ने मीडिया पर कब्जा जमा लिया है, और ये पूंजीपति सत्ताधारी दलों के साथ गठजोड़ में हैं। नतीजतन, सोशल मीडिया को छोड़कर स्वतंत्र मीडिया की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। तीसरा, वर्तमान सत्ता ने मीडिया को नियंत्रित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं—चाहे वह प्रलोभन हो, दबाव हो, या दंड।इमरजेंसी की सेंसरशिप आज के दौर में बच्चों का खेल लगती है। तब सेंसरशिप नकारात्मक थी, जो सरकार की आलोचना को रोकने पर केंद्रित थी। आज का मीडिया नियंत्रण आक्रामक है, जो सत्ता के लिए हथियार की तरह काम करता है। इसे ‘गोदी मीडिया’ का नाम मिला है, लेकिन यह शब्द भी इसकी आक्रामकता को पूरी तरह बयां नहीं कर पाता। यह मीडिया न केवल सत्ता की गोद में बैठता है, बल्कि उसके इशारे पर विपक्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों, और यहाँ तक कि मानवीयता के खिलाफ भी भौंकता और काटता है।2024 के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का ‘चार सौ पार’ का नारा ढाई सौ सीटों से नीचे सिमट गया, और वह बहुमत खो बैठी। यह झटका 1977 या 2004 जितना गहरा नहीं था, लेकिन यह मीडिया के बदले चरित्र को दर्शाता है। आज का गोदी मीडिया न केवल सत्ता की सेवा करता है, बल्कि हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का सक्रिय औजार भी है। इमरजेंसी में मीडिया सत्ता के खिलाफ था; आज का मुख्यधारा मीडिया सत्ता का हथियार बन चुका है। यह तानाशाही का मीडिया नहीं, बल्कि उससे एक कदम आगे, नव-फासीवादी ताकतों का मीडिया है।
(लेखक:- हरि शंकर पाराशर)




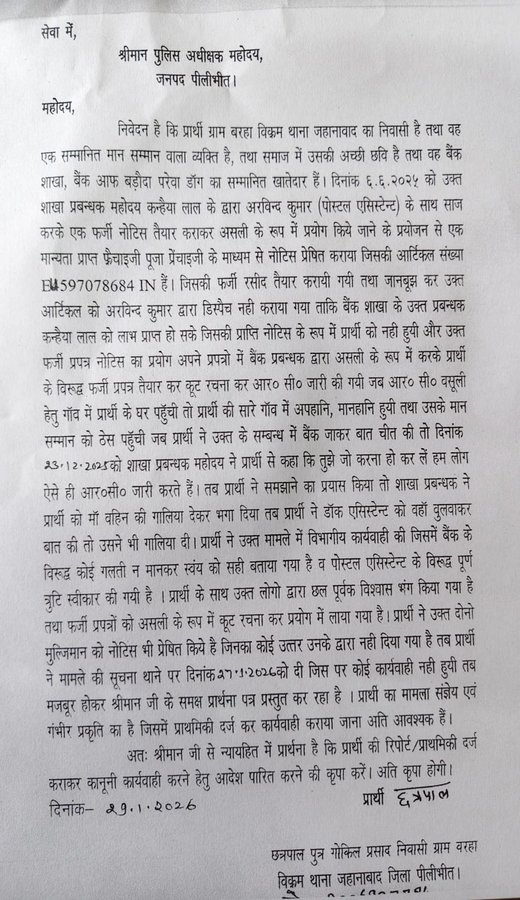



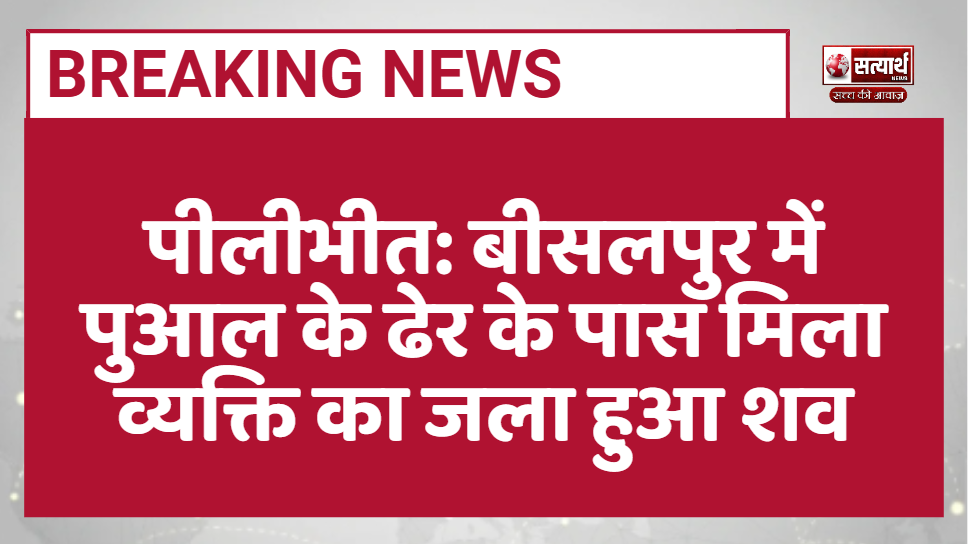






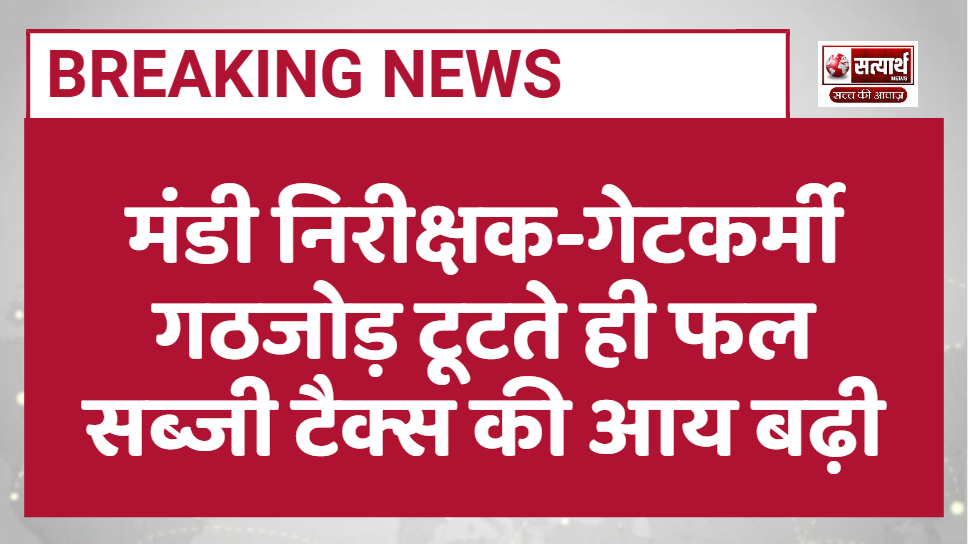
Leave a Reply